The crisis will keep coming ... Never give up
If your son or daughter is studying, then this article is for you
लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती...
जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य को सही या गलत ढालने में मदद करता हैं. ये जान लीजिये की अच्छी-बुरी चीजें, असफलता किसी भी क्षेत्र में मिल सकती हैं. सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, आप को इसे बनाना होता हैं...
दूसरी ओर आय.आय.टी. पढ़ रहे और उसकी तैयारी कर रहे बच्चों में फैलने वाली निराशा के दुष्प्रभाव भी उभरकर सामने आ रहे हैं. इस निराशा के पीछे की मानसिकता की तह तक जाने की कोशिश की हैं...
जाहिर हैं इस शैक्षिक उन्नति के दौर में हम भारतियों की अंतर्निहित प्रतिभा (In-built talent) को और संवारा, सजाया और हमारे सपनों को ऊंची उड़ान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिसके चलते आज कई इंजीनियर, डॉक्टर दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें गूगल के सी.इ.ओ. सुन्दर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सी.इ.ओ. सत्य नडेला के नाम एक मिल का पत्थर सिद्ध हुआ हैं. हर भारतीय को गर्व हैं की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन लोगों ने हमारे देश का वर्चस्व बढ़ाया हैं.
मगर इन दो नामो को हम भारतीय किस नजर से देखते हैं? उसके बाद हमारी मानसिकता और उससे पनप रहे दुष्परिणामों पर चर्चा करेंगे.
गूगल सर्च में सिर्फ सुन्दर पिचाई नाम टाइप करें, सबसे पहला सजेशन
Sundar Pichai salary आता है.
जिसका मतलब हैं लोग सुन्दर पिचाई की सैलरी के बारे में सबसे ज्यादा सर्च करते हैं.
गूगल में सुन्दर पिचाई की-वर्ड को प्रतिमाह औसतन मिलने वाले सर्च देखें...
sundar pichai salary 40,500 (प्रतिमाह मिलने वाले औसतन सर्च)
sundar pichai education 27,100 (प्रतिमाह मिलने वाले औसतन सर्च)
sundar pichai biography 4,400 (प्रतिमाह मिलने वाले औसतन सर्च)
यहीं बात सत्या नडेला के बारे में भी गूगल चेक करोगे तो करीब इसी तरह के आंकड़े आपको मिलेंगे.
ऐसे काफी सारे नाम होंगे जो अपने सपनों की उचाई छु रहे होंगे.
हमारा सफल लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण क्या हैं? या यूँ कहें की हमारा दृष्टिकोण ही हमारा अंजाम हैं.
हम पहले सुन्दर की सैलरी देखते हैं, फिर उनका एजुकेशन और सबसे आखिर में उनका चरित्र, संघर्ष पढ़ते हैं. क्या आपको लगता नहीं की यहाँ गंगा उलटी बह रही हैं?
अगर सुन्दर जैसे बनना हैं तो पहले उनके चरित्र, संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, फिर उनकी पढ़ाई और उसके लिए ली गयी मेहनत से सीख लेनी चाहिए, अगर उनसे हम कुछ सीखते हैं तो सैलरी अच्छी मिलेगी ही...
क्या उनके जैसे लोगों की सैलरी के प्रति हमारे संकीर्ण दृष्टिकोण से हम कुछ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी जीवनशैली भी उनकी जैसी बने?
अच्छी नौकरी और बड़ी सैलरी के चक्कर में हमारे युवा कहीं निराशा का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्या यही निराशा उन्हें अपने आप को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर रही हैं? विगत कुछ सालों से ये बात उभरकर सामने आने लगी हैं. किशोर उम्र के बच्चों में ये मानसिकता ज्यादा दिखती हैं मगर उच्च शिक्षा लेने वाले युवा भी इनमे बड़ी मात्रा में शामिल हैं. किसी भी युवा को अपने आप ख़त्म करते हुए देखना, बेहद दुखद बात हैं.
कुछ दिन पूर्व आय.आय.टी., हैदराबाद के छात्र मार्क एंड्र्यू चार्ल्स ने अपने हॉस्टल के कमरे आत्महत्या कर ली. इस साल इस संस्था में यह दूसरी आत्महत्या है. उसकी डायरी में लिखा एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले और इस "असफलता" का कोई भविष्य नहीं हैं.
असफलता या मनचाही बात, ना होने के डर से जीवन को समाप्त करना ये कहाँ तक उचित हैं?आत्महत्या अगर सभी असफलताओं का परिणामस्वरूप होता तो काफी असफलताएं मिलने के बाद भी जीवन में ऊंचाइयों को छुआ क्या वह लोग वहां पहुँच पाते?
ऐसे कई उदहारण दे सकते हैं...
अमिताभ बच्चन... जिनको उनके आवाज की वजह से आकाशवाणी ने नौकरी देने के लिए से मना किया, उसी आवाज ने उनको फ़िल्मी दुनिया का सितारा बना दिया. वाल्ट डिज्नी, थॉमस एडिसन, धीरूभाई अम्बानी..... कई लोग हैं जिनकी प्रेरणा से लाखो लोग अविरत संघर्ष कर अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहते हैं.
अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी... यही सबकुछ हैं ऐसा मानना अपने आप से धोखा हैं. जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने पर भी कई लोग दुखी होते हैं.... क्यूंकि वहां मनचाहा काम करने नहीं मिलता. बोलते हैं सबकुछ हैं मगर जॉब सटिस्फैक्शन नहीं हैं... युवाओं के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में पढ़े लिखे बच्चों के लिए कई सारे अवसर हैं. वहां वह अपनी प्रतिभा दिखाएं. जीवन एक लड़ाई हैं, संघर्ष हैं.... ओर आत्महत्या करना इस संघर्ष से भाग जाना हैं.
फिर भी ये आत्महत्या की मानसिकता कहाँ से पनपती हैं?
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से शैक्षणिक तनाव और इसके प्रभाव के संदर्भ में, दुनिया भर में छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं (Policy makers) के बीच एक गंभीर मुद्दा बन गया है.
वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि भारत में उच्च माध्यमिक छात्रों के 70% शैक्षणिक तनाव का अनुभव करते हैं. बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए माता-पिता का दबाव ज्यादातर शैक्षिक तनाव के लिए जिम्मेदार पाया गया, जैसा कि 70% छात्रों द्वारा बताया गया. अधिकांश माता पिता ने कक्षा में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले छात्र के प्रदर्शन की तुलना करके अपने बच्चों की आलोचना की. नतीजतन, दोस्ती के बजाय, सहपाठियों में प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित होने लगती हैं.
माध्यमिक स्कूल के छात्रों (10 वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा) और वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्रों (12 वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा) में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा हैं।
लगातार अकादमिक और पाठ्येतर (co-curricular) दोनों गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने बच्चे को माता-पिता द्वारा प्रेरित किया जाता है.
माता-पिता अपने बच्चों पर सफल होने के लिए दबाव डालते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के कल्याण के लिए और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना मानते हैं. भारत में समग्र बेरोजगारी की स्थिति ने भी माता-पिता को अपने बच्चों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए दबाव डालने के लिए बाध्य किया है.
कुछ माता-पिता अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आधे से अधिक माता-पिता अपने बच्चे के लिए 3 से 4 निजी ट्यूटर या उससे भी अधिक नियुक्त करते हैं. उन दिनों में जब कोई शैक्षणिक ट्यूशन नहीं होती, कला या संगीत पाठ होते हैं. छात्रों को मुश्किल से टीवी देखने, खेलने या पड़ोसियों से खुलकर बातचीत करने या पर्याप्त नींद लेने के लिए भी समय नहीं मिलता है. जिसकी वजह से उनके अंदर छिपी प्रतिभा न्याय नहीं मिल पाता. स्वाभाविक रूप से इस तरह के छात्रों को परीक्षा के दबाव के बढ़ने पर घबराहट होती है.
क्या उच्च शिक्षा लेते समय भी बच्चो पर यही दबाव होता हैं?
आय.आय.टी. दिल्ली के छात्र सक्षम गर्ग कहते हैं, की बहुत से लोग इस विचार के होते हैं कि जीवन एक अच्छे आईआईटी में प्रवेश करने के बाद जिंदगी में सुकून ओर शांति रहती होती. मैं उसी भावना के साथ यहाँ आया था. मगर जब मैंने यहां लोगों को देखा, तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया. हाँ ... लोग दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी श्रेणी प्राप्त कर रहे हैं. वे हर रोज 10-12 घंटे अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन, वे कक्षाओं के बाद अधिकांश समय के लिए अध्ययन करते हैं. वे या तो पुस्तकालय में या हॉस्टल के वाचनालय में पाए जाते हैं. मगर यहाँ खेलों के मैदान एवं क्लब्स भी होते हैं. यहाँ प्रतिस्पर्धा बहोत हैं ओर यहाँ आने के बाद पढाई की शुरुआत होती हैं, ना की ख़त्म.
तो क्या औसतन छात्र के लिए आईआईटी में जाना कठीण हैं?
आय.आय.टी. दिल्ली के छात्र नमन बंसल कहते हैं की, आप किसी एक क्षेत्र में अच्छा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप औसत छात्र हैं या औसत से कम छात्र हैं. यह उस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा के बारे में है (मैं गणित में अच्छा था, इसलिए जेईई एडवांस क्लियर किया). लेकिन मैं रॉट लर्निंग में अच्छा नहीं था इसलिए बोर्ड्स या स्कूल की अन्य परीक्षाओं में असफल रहा. खुद पर भरोसा रखें. लेकिन, अति आत्मविश्वास न करें. आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक पतली रेखा है.
अपने लक्ष्य की स्पष्टता, आपको अपनी पसंद के अनुसार प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य चीजों को छोड़ना होगा. हमेशा अपनी विफलता से सीखे. मैंने यह गुणवत्ता कक्षा 10 में VMC प्रवेश के बाद सीखी और इसे अपने JEE एडवांस्ड (गणित के पेपर में केवल 1 गलती की). JEE की परीक्षा ऐसी हैं है जहाँ 10% अंकों का मतलब है पैन इंडिया स्तर पर 3000 रैंक का अंतर (तो, यह परीक्षा में आपके MISTAKE के बारे में है. इसलिए, इसे सुधारें और इसमें शामिल हो जाइये हैं). सफल होना आपकी पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह आपके जीवन के प्रति ATTITUDE पर निर्भर करता है.
जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य को सही या गलत ढालने में मदद करता हैं. ये जान लीजिये की अच्छी-बुरी चीजें, असफलता किसी भी क्षेत्र में मिल सकती हैं. सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, आप को इसे बनाना होता हैं... अच्छे-बुरे हालात से लड़ना होगा. जो बुरे हालात रहे हैं उनसे एक एक असफलता का बदला लेना होगा. इसलिए छोटे सपने ना देखें... किसी ने खूब कहा हैं, अगर बड़ा सपना नहीं देखोगे, तो जिंदगी भर कोई और उसका सपना बड़ा करने के लिए तुम्हे इस्तेमाल करेगा.
जय हिन्द
वन्दे मातरम





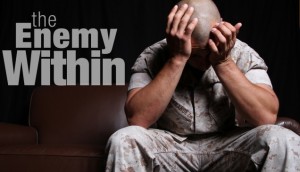











Post A Comment
No comments :